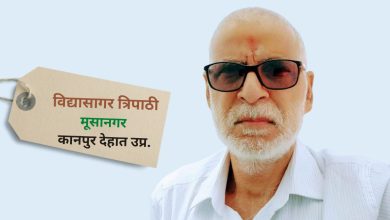हिंदीतर जैसे कि अंग्रेज़ी के विरुद्ध जिहादी या कट्टर मानसिकता तो ठीक नहीं है लेकिन मातृभाषा यानी हिंदी या अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं को कुचलकर किसी अन्य बाह्य भाषा पर निर्भरता तार्किक नहीं है।
हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिनका संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिंदी में दिया गया भाषण -” भारत के बाहर हिंदी बोलना आसान है लेकिन भारत में नहीं।” एक तरफ तो हिंदी के विकास को दिखता तो दूसरी तरफ़ प्रश्नचिन्ह भी लगाता। चूँकि न तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन पाई और न ही संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद व्यावहारिक रूप में एक मात्र राजभाषा। इसका मुख्य कारण रहा अतार्किक राजनीतिक गतिरोध। उल्लेखनीय है रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था,’ प्रत्येक के लिए अपनी मातृभाषा और सबके लिए हिंदी। यही सोच भारतीय भाषाओं को मजबूत करेगी।’ कुछ इसी आधार पर हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति की 37वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृहमन्त्री अमितशाह ने कहा हिंदी भारत की सम्पर्क भाषा बने; यह स्थानीय भाषा के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के विकल्प के रूप में स्वीकार की जाए। यद्यपि इसमे अंतर्निहित है कि हिंदी की छतरी तले सभी भाषाएँ ससम्मान पुष्पित एवं पल्लवित होंगी। लेकिन दक्षिण एवं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हिंदी के विरुद्ध विरोध तूल पड़ने लगा। यह राजनीतिक हित से प्रेरित है जोकि सिर्फ़ विरोध के लिए किया गया विरोध मालूम पड़ता है। उल्लेखनीय है, स्वाधीनता आंदोलन के समय तो सभी क्षेत्रों के नेताओं ने हिंदी के पक्ष में खुलकर राय रखी थी जैसे कि पंजाब में लाजपतराय, महाराष्ट्र में सावरकर एवं तिलक, गुजरात में सरदार पटेल, दक्षिण भारत में सी राजगोपालचारी आदि। लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आंतरिक राजनीतिक जटिलताओं के चलते हिंदी राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर विरोध होने लगे। और आज़ादी के बाद से अब तक ऐसे हालात नहीं बन पाए कि प्रभावी रूप से राष्ट्रभाषा का मुद्दा उठाया जा सका। एक कारण यह भी रहा की 1967 गठबंधन दौर शुरू हो गया। सारी राजनीतिक पार्टियाँ इस मुद्दे से बचती रहीं।
महात्मा गांधी का मत था- “ हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए।” इसके अपने पर्याप्त तर्क भी है- भारत के 10 राज्यों की प्राथमिक भाषा हिंदी है जोकि देश की आबादी का 42 प्रतिशत हैं तथा 30 प्रतिशत लोगों की हिंदी द्वितीयक भाषा है। यानी कुछेक प्रतिशत लोगों को छोड़कर लगभग सभी भारतीय हिंदी पढ़ने व समझें में सक्षम हैं। यह सम्पर्क भाषा की भी सभी कसौटियों पर खरी उतरती है। अफ़सोस है कि राजनीतिक गतिरोध के चलते आज तक हिंदी पूर्ण रूप से सम्पर्क भाषा नहीं बन पाई।
सर्वविदित है हिंदी हमारे देश के स्वर्णिम अतीत का हिस्सा रही है। राष्ट्र निर्माण में भी हिंदी के अहम योगदान को नहीं भुलाया जा सकता; जिसने पूरे देश के लोगों को एक सूत से बांधकर स्वाधीनता की राह को आसान किया। साथ ही देश की अनेक मोती रूपी भाषाएँ एवं बोलियों को एक माला में पिरोने का काम करती आयी है। लेकिन अगर आज़ादी के बाद की स्थिति पर गौर करें तो निराशा हाथ लगती है। राजभाषा के मुद्दे पर आज़ादी के तुरंत बाद के समय को संक्रमण काल माना संविधान सभा में सहमति बनी कि आगामी 15 सालों तक सरकारी कार्यों में हिंदी के साथ अंग्रेज़ी की मदद ली जा सकती है। तथा 1965 के बाद से स्वतः सरकारी कामकाज की हिंदी एक मात्र राजभाषा होगी। समय समाप्ति के कुछ वर्ष पूर्व ही हिंदी विरोधी आंदोलन होने लगे स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि अंग्रेज़ी के यथावत प्रयोग को संविधान संशोधन के ज़रिए भविष्य कि लिए स्वीकृति दे दी गई। यह निर्णय कुछ यूँ रहा जैसे कि हिंदी रूपी वृक्ष को ज़मीन से उखाड़ कर गमले में लगा दिया गया हो। यानी भाषा तो रही लेकिन विकास सम्भावनाएँ सीमित गईं। और व्यवहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, क़ानून आदि जीवन का हर क्षेत्र अंग्रेज़ीमय हो चला। जिसके चलते हिंदी उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बन सकी। यही नहीं अब प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के रूप में भी तेज़ी से गिरावट होती जा रही है।
अधिकांश भारतीय परिवारों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। जबकि शुरुआती शिक्षा बढ़ता अंग्रेज़ी माध्यम; यह विरोधाभास बच्चों में सीखने की क्षमता को बाधित कर रहा है। इसका परिणाम विज्ञान, तकनीकी आदि क्षेत्रों में मौलिक चिंतन हतोत्साहित हो रहा है। कारण है व्यक्ति सपने मातृभाषा में ही देखता है यदि उसे उसी भाषा में पूरा करने का अवसर मिले तो सफलता की सम्भावना कई गुना बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि भाषा में ही संस्कृति बसती है। अंग्रेज़ीकरण के चलते अपनी संस्कृति ही परायी लगने लगी, जीवन मूल्य ही संदेह के घेरे में आ गये।
वर्तमान वैश्विक युग में सभी भाषाओं का अपना महत्व है। अहिंदी जैसे कि अंग्रेज़ी के विरुद्ध जिहादी या कट्टर मानसिकता तो ठीक नहीं। लेकिन वर्तमान भारतीय परिदृश्य को देखते हुए लगता है कि अंग्रेज़ी का वर्चस्व बढ़ रहा है यदि ऐसे महत्वपूर्ण प्रयासों पर गतिरोध उत्पन्न किया जाता रहा तो आने वाले 400 से 500 वर्षों में अंग्रेज़ी सम्पर्क भाषा होने का दावा कर सकती है। ध्यान रहे जब भाषा समाप्त होती है उसके साथ सोंच का एक तरीक़ा समाप्त हो जाता है यानी विचारधारा समाप्त हो जाती है। साथ ही मूल्य एवं संस्कृति प्रभावित होती है। ज़रूरी हो जाता है कि सभी राज्य अपने छुद्र राजनीतिक हितों से हटकर हिंदी के विकास के लिए तार्किक रूप से चिंतन करें।
मोहम्मद ज़ुबैर
MSW (Gold Medalist)
इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
Discover more from अमन यात्रा
Subscribe to get the latest posts sent to your email.